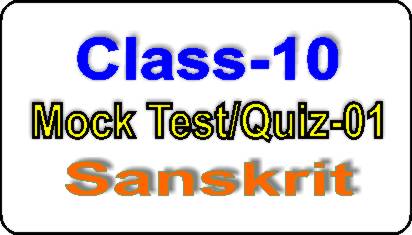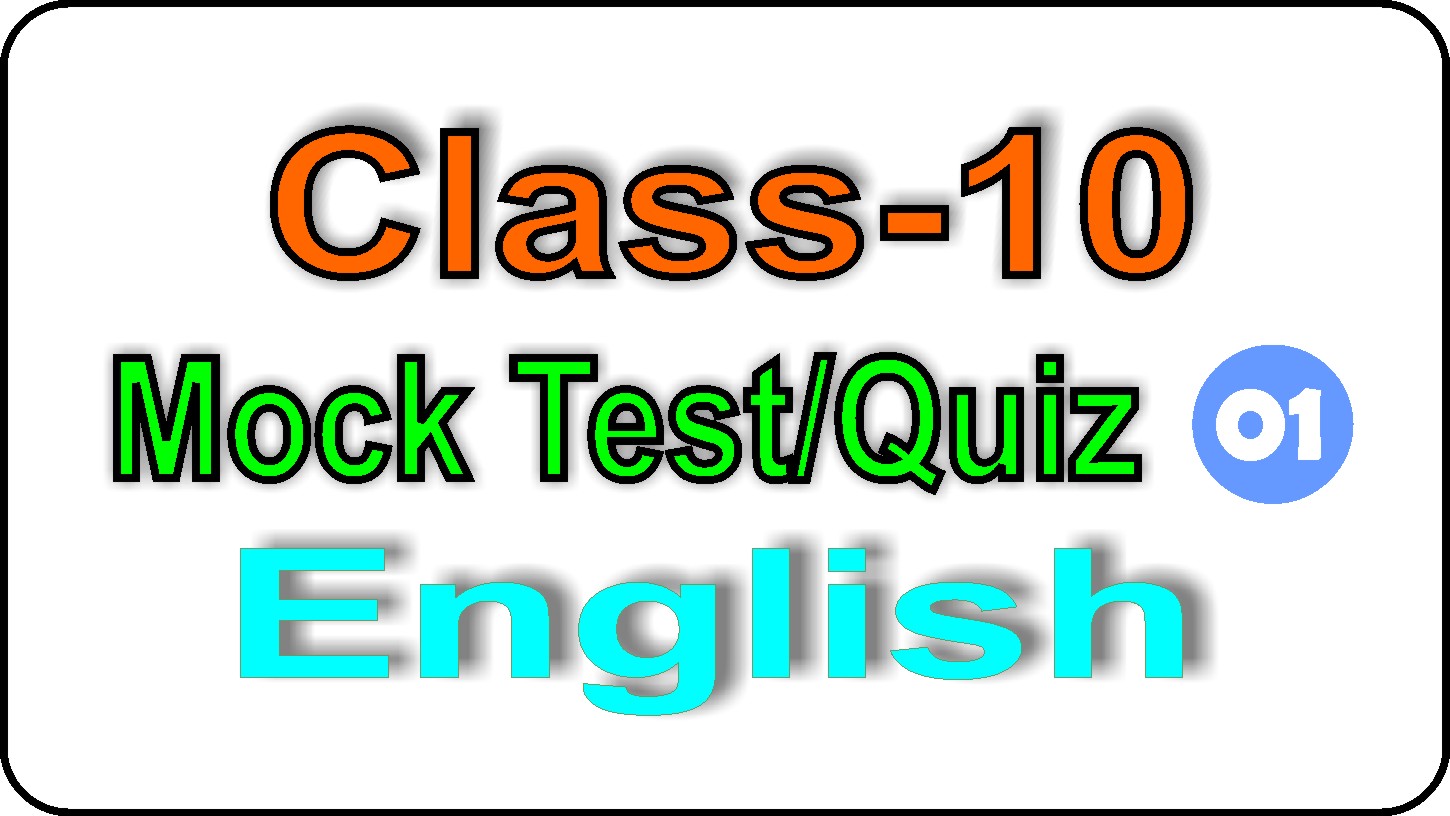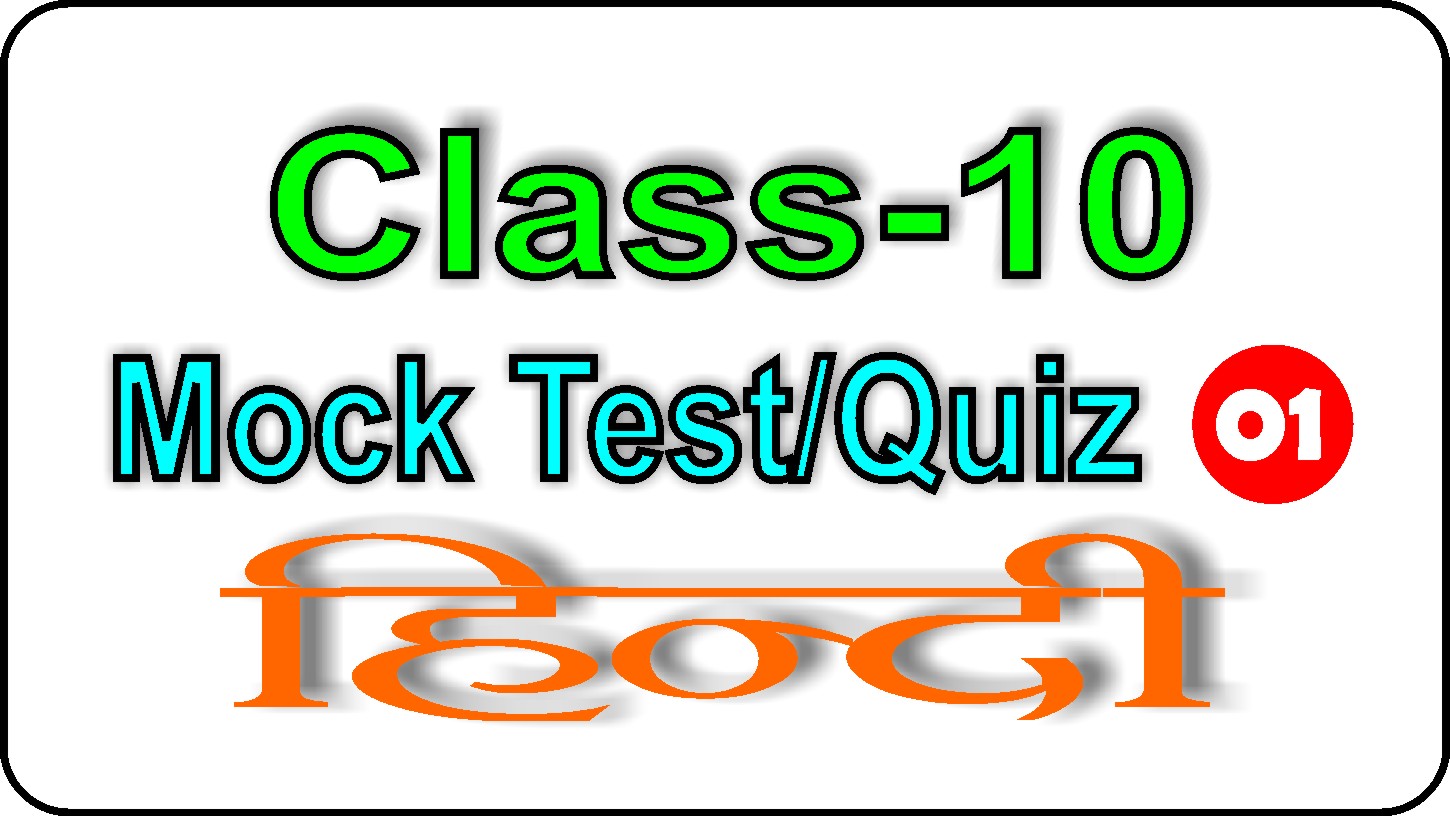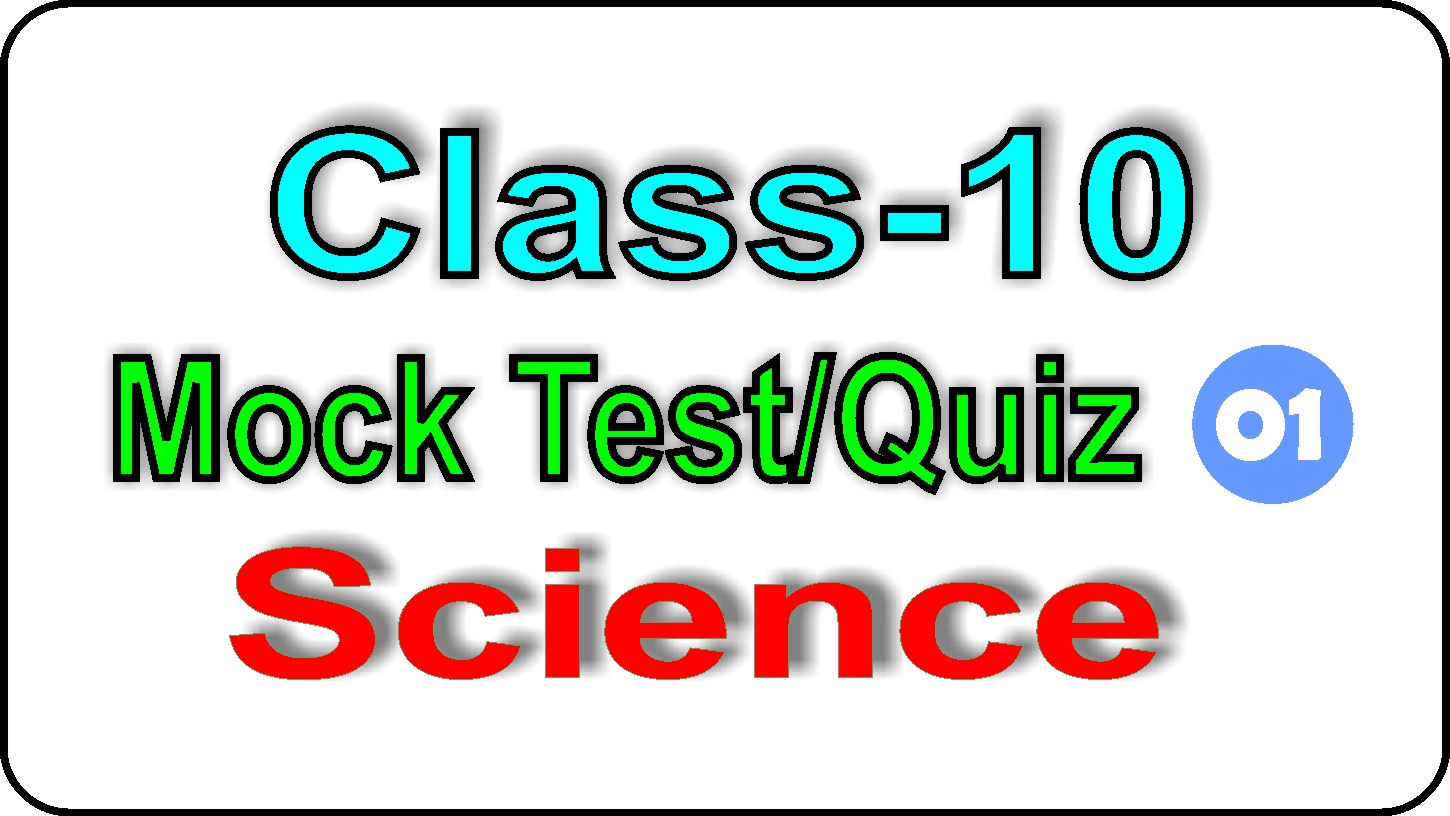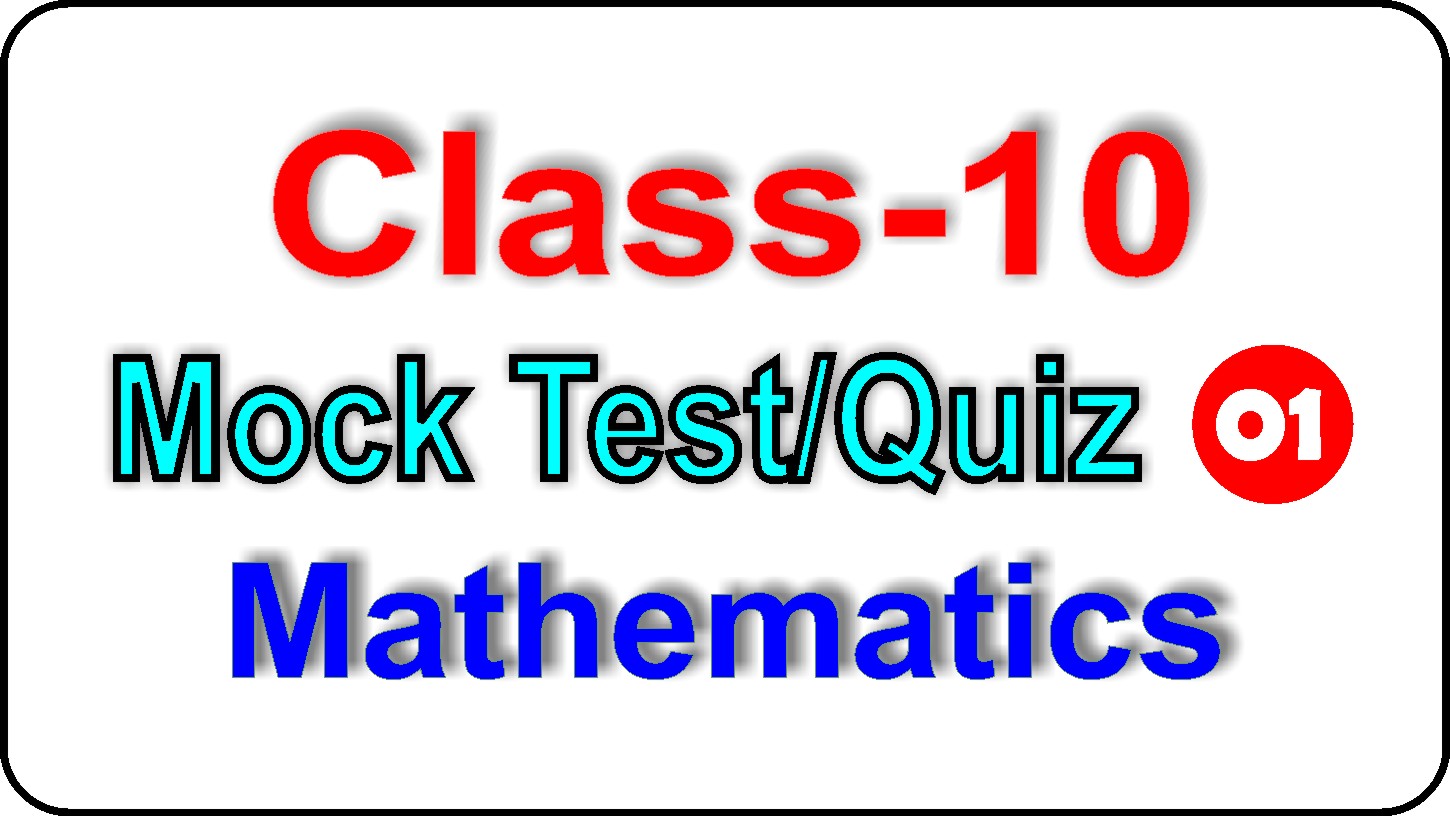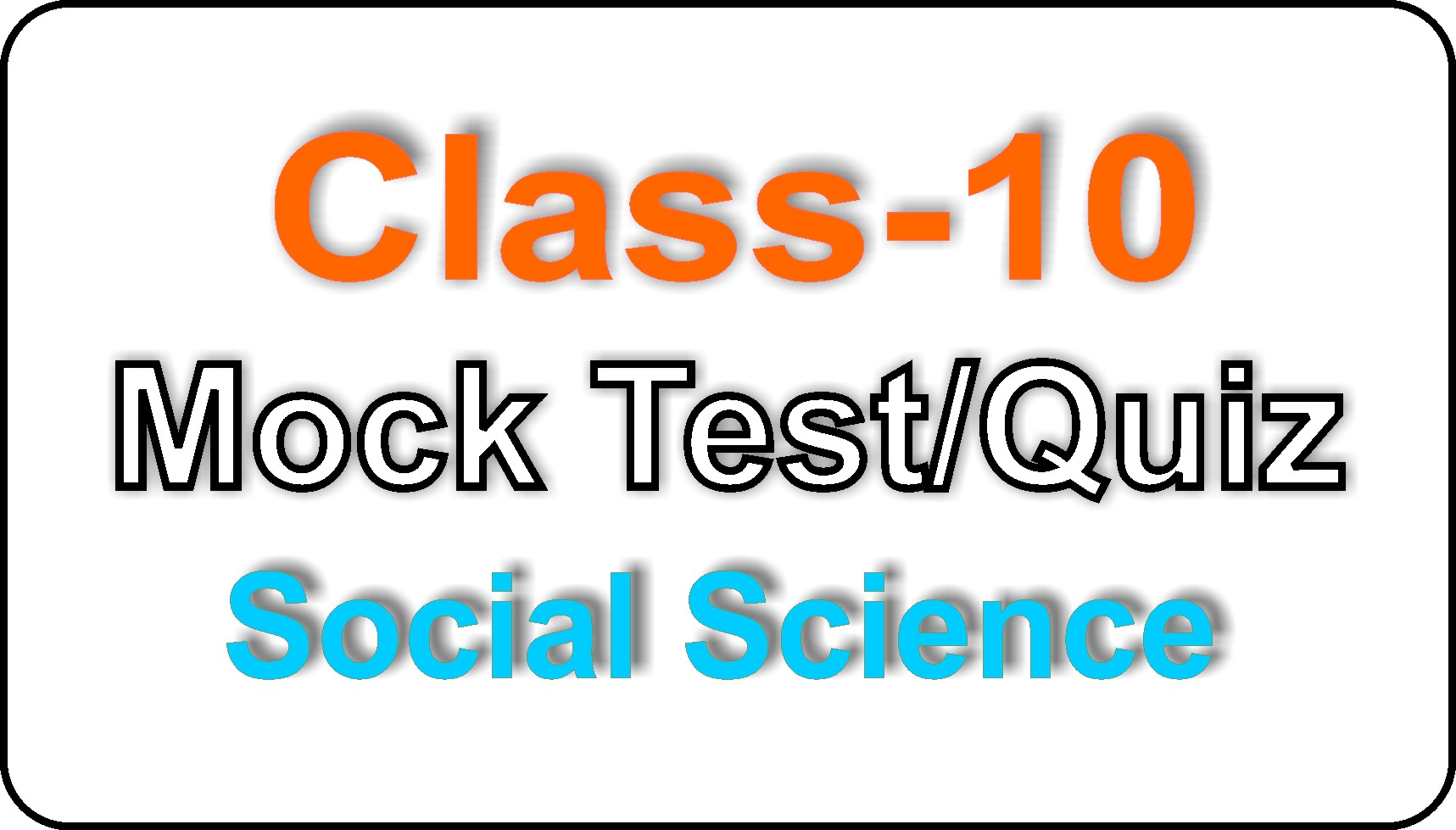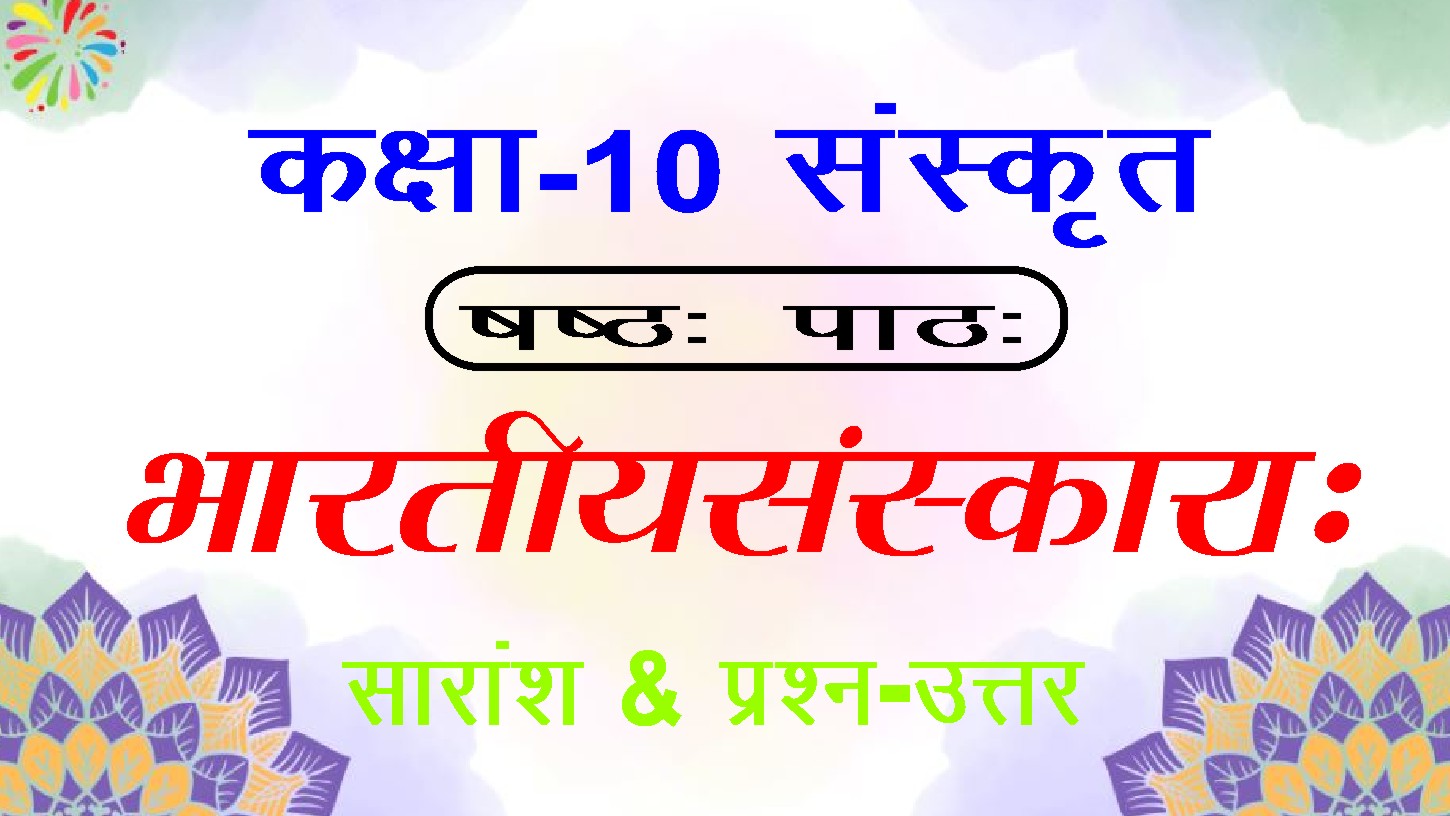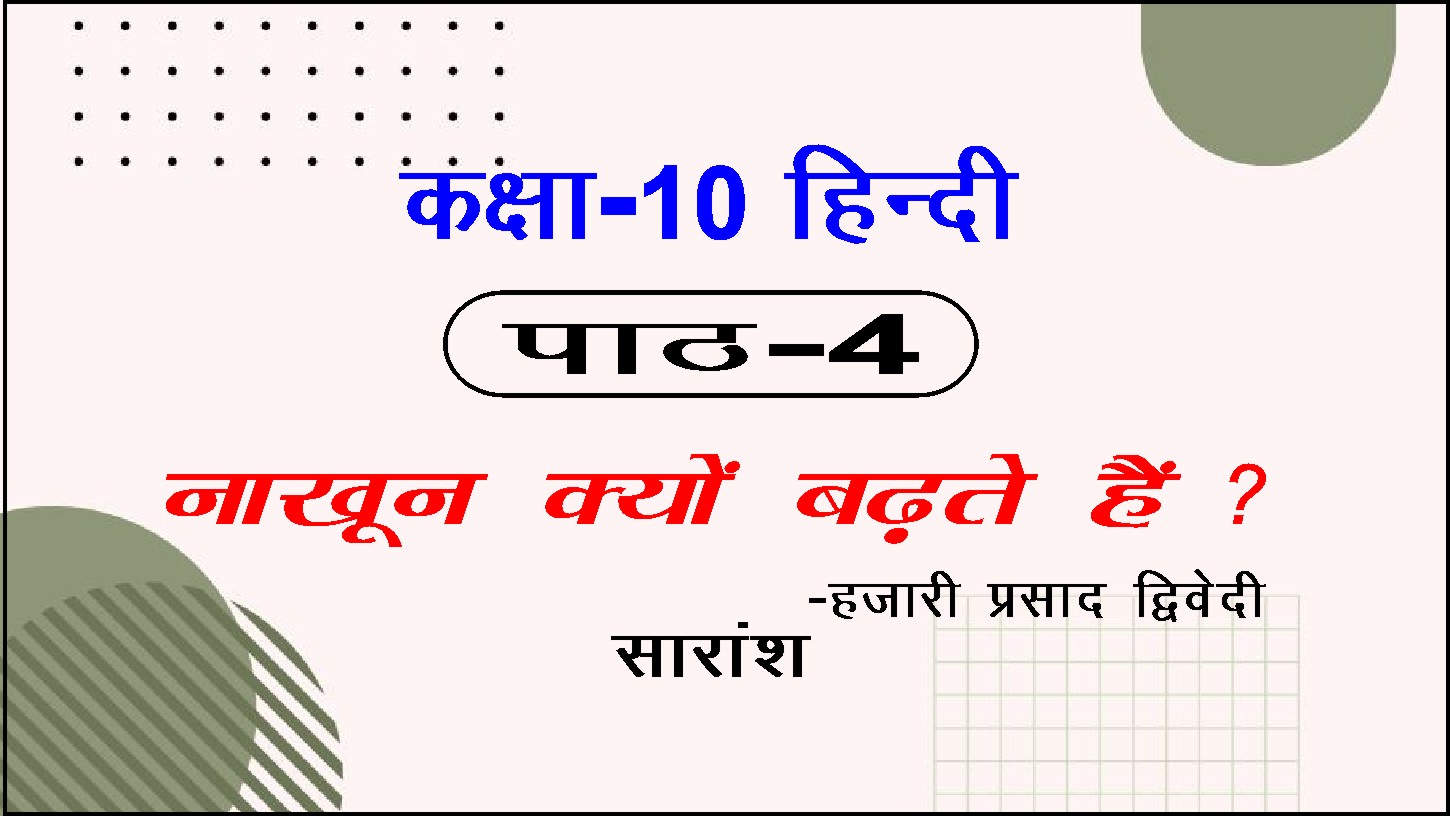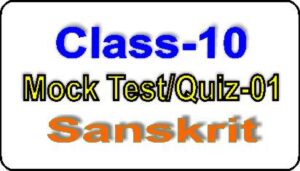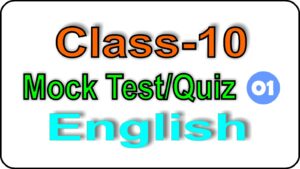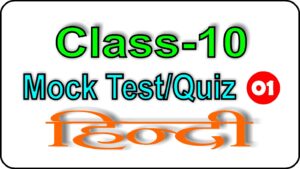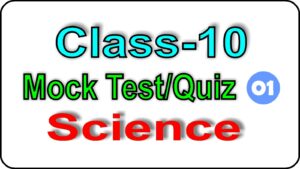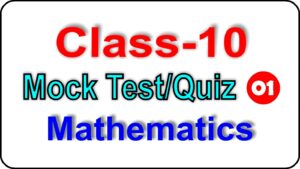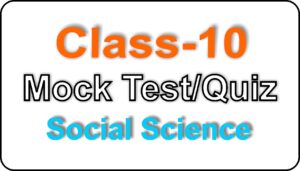दोस्तों इस पोस्ट के माध्यम से मैं Bihar Board 10th Class Sanskrit Chapter 7 नीतिश्लोकाः पाठ का हिन्दी अनुवाद बहुत ही आसान भाषा में समझने का प्रयास किया हूँ। साथ ही कुछ चुनिंदा प्रश्न जो हर बार परीक्षा में पूछा जाता हैं और उसका उत्तर हिन्दी में लिखना होता हैं उसे भी शामिल किया हूँ उम्मीद करता हूँ की आपको काफी पसंद आएगी। अगर आपलोग गणित विषय की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे Youtube Channel Unlock Study पर जाकर अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं।
सप्तमः पाठः
नीतिश्लोकाः
(अयं पाठः सुप्रसिद्धस्य ग्रन्थस्य महाभारतस्य उद्योगपर्वणः अंशविशेष (अध्यायाः ३३-४०) रूपायाः विदुरनीतेः संकलितः। युद्धम् आसन्नं प्राप्य धृतराष्ट्रो मन्त्रिप्रवरं विदुरं स्वचित्तस्य शान्तये कांश्चित् प्रश्नान् नीतिविषयकान् पृच्छति । तेषां समुचितमुत्तरं विदुरो ददाति । तदेव प्रश्नोत्तररूपं ग्रन्थरत्नं विदुरनीतिः। इयमपि भगवद्गीतेव महाभारतस्याङ्गमपि स्वतन्त्रग्रन्थरूपा वर्तते।)
अर्थ- यह पाठ सुप्रसिद्ध ग्रन्थ महाभारत के उद्योग पर्व का अंश विशेष (अध्याय 30-40) रूप से विदुरनीति से संकलित है।
युद्ध को नजदीक जानकर धृतराष्ट्र महामंत्री विदुर को अपने चित्त के शान्ति के लिए नीति विषय के कुछ प्रश्नों को पूछते हैं। उन सभी को समुचित उतर विदुर देते हैं। तब से ही प्रश्न उतर रूप ग्रन्थरत्नं विदुरनीति है। यह भी भगवद्गीता और महाभारत का अंग स्वतंत्र ग्रन्थ रूप है।
यस्य कृत्यं न विघ्नन्ति शीतमुष्णं भयं रतिः ।’
समृद्धिरसंमृद्धिर्वा स वै पण्डित उच्यते ॥१॥
अर्थ- जिसके करने में न विघ्न, शीत, उष्ण, भय, आनन्द, समृद्धि, असमृद्धिः है वह पण्डित कहा जाता है।
तत्त्वज्ञः सर्वभूतानां योगज्ञः सर्वकर्मणाम् ।
उपायज्ञो मनुष्याणां नरः पण्डित उच्यते ॥२॥
अर्थ -सभी प्राणियों के रहस्य को जानने वाला सभी कर्मों के कौशल जानने वाले मनुष्यों के उपाय को जानने वाला नर पण्डित कहा जाता है।
अनाहूतः प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते ।
अविश्वस्ते विश्वसिति मूढ्चेता नराघुमः ॥३॥
अर्थ -‘बिना बुलाये हुए आनेवाला विना पुछे हुए बोलने वाला अविश्वसनीय व्यक्ति पर विश्वास करने वाला मनुष्यों में नीच मूर्ख हृदय वाला है।
एको धर्मः परं श्रेयः क्षर्मका शान्तिरुत्तमा ।
विदूयैका परमा तृप्तिः अहिंसका सुखावहा ॥३॥
अर्थ- एक ही धर्म सर्वश्रेष्ठ है। एक क्षमा उत्तम शान्ति है। एक विद्या श्रेष्ठ आत्मसंतुष्टि है। एक अहिंसा सुख देने वाली है।
त्रिविधं नरकस्वेदं द्वारं नाशनमात्मनः ।
कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत् त्रयं त्यजेत् ॥५॥
अर्थ -तीन प्रकार के नरक के द्वार हैं काम, क्रोध तथा लोभ। इससे आत्मा नष्ट हो जाती है। इन तीनों को छोड़ देना चाहिए।
पडू दोषाः पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिच्छता ।
निद्रा तन्द्रा भयं क्रोध आलस्यं दीर्घसूत्रता ॥६॥
अर्थ- ऐश्वर्य को चाहते हुए पुरुषों से यह छः दोष निद्रा, तन्द्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घसूत्रता से हटना चाहिए।
सत्येन रक्ष्यते धर्मो विद्या चोगेन रक्ष्यते ।
मृजया रक्ष्यते रूपं कुलं वृत्तेन रक्ष्यते ॥७॥
अर्थ- धर्म की रक्षा सत्य के द्वारा, विद्या की रक्षा योग के द्वारा, रूप की रक्षा स्वच्छता से और कुल की रक्षा शील से।
सुलभाः पुरुषा राजन् सततं प्रियवादिनः ।
अप्रियस्य तु पध्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः ॥८॥
अर्थ- हे राजन् ! समय प्रिय बोलने वाला पुरूष सुलभ है। किन्तु अप्रिय हितकर बचन बोलने और सुनने वाला दुर्लभ हैं।
पूजनीया महाभागाः पुण्याश्च गृहदीप्तयः ।
स्वियः श्रियो गृहस्योक्तास्तस्मादक्ष्या विशेषतः ॥९॥
अर्थ- घर की लक्ष्मी, घर को प्रकाशित करने वाली, पुण्या, महाभागा, स्त्री, पूजनीय हैं। वह विशेष रूप से रक्षा करने योग्य हैं।
अकीर्ति विनयो हन्ति हन्त्यनर्थ पराक्रमः ।
हन्ति नित्यं क्षमा क्रोधमाचारो हन्त्यलक्षणम् ॥१०॥
अर्थ-विनम्रता अपयश को नाश करता है, पराक्रम अनर्थ को नाश करता है, क्षमा प्रतिदिन क्रोध को नाश करता है, आचरण कुलक्षण को नाश करता है।
अन्वया
यस्य कृत्यं शीतम्, उष्णं, भयं, रतिः, समृद्धि, असमृद्धिः वा
(च) न विघ्नन्ति सः वै पण्डित उच्यते ॥१॥
अर्थ-जिसके करने में न विघ्न, शीत, ऊष्ण, भय, आनन्द, समृद्धि, असमृद्धि है वह पं० कहा जाता है।
सर्वभूतानां तत्त्वज्ञः सर्वकर्मणां योगज्ञः मनुष्याणाम्
(च) उपायज्ञः नरः पण्डितः उच्यते ॥२॥
अर्थ-सभी प्राणियों के रहस्य को जाननेवाला, सभी कर्मों के कौशल को जाननेवाला सभी मनुष्यों के उपाय को जाननेवाला नर पण्डित कहा जाता है।
मूढचेता नराधमः अनाहूतः प्रविशति, अपृष्टः (अपि) बहु भाषते,
अविश्वस्ते (च) विश्वसिति ॥३॥
अर्थ-बिना बुलाये हुए आनेवाला विना पूछे हुए बोलने वाला, अविश्वसनीय व्यक्ति पर विश्वास करने वाला मनुष्यों में नीच मूर्ख हृदय वाला है।
एकः (एव) धर्मः परं श्रेयः, एका (एव) क्षमा उत्तमा शान्तिः, एका विद्या परमा
तृप्तिः, एका अहिंसा (च) (परमा) सुखावहा (भवति) ।॥४॥
अर्थ- एक ही धर्म सर्वश्रेष्ठ है। एक क्षमा उत्तम शान्ति है। एक विद्या श्रेष्ठ आत्मसंतुष्टि है। एक अहिंसा सुख देनेवाली है।
नरकस्य इदम् त्रिविधं द्वारं कामः, क्रोधः तथा लोभः (चेति)।
तस्मात् आत्मनः नाशनम् एतत् त्रयं त्यजेत् ॥५॥
अर्थ- नरक जाने का तीन रास्ता है। काम, क्रोध, तथा लोभ। इससे आत्मा नष्ट हो जाती है। इन तीनों को छोड़ देना चाहिए।
भूतिम् इच्छता पुरुषेण इह निदा, तन्द्रा, भयं, क्रोधः, आलस्यं,
दीर्घसूत्रता (च) षड् दोषाः हातव्याः ॥६॥
अर्थ- ऐश्वर्य को चाहनेवाले पुरूष छः दोष दूर होना चाहिए-निद्रा, तन्द्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घसूत्रता।
धर्मः सत्येन रक्ष्यते, विद्या योगेन रक्ष्यते, रूपं मृजया रक्ष्यते,
कुलं (च) वृत्तेन रक्ष्यते ॥७॥
अर्थ- धर्म की रक्षा सत्य के द्वारा, विद्या की रक्षा योग के द्वारा, रूप की रक्षा स्वच्छता से और कुल की रक्षा शील से।
हे राजन् ! सततं प्रियवादिनः पुरुषाः सुलभाः (सन्ति) तु अप्रियस्य पथ्यस्य वक्ता
श्रोता च दुर्लभः (अस्ति) ॥८॥
अर्थ- हे राजन् ! हरेक समय प्रियबोलने वाला पुरूष सुलभ है। किन्तु अप्रिय हितकर बचन बोलने और सुनने वाला दुर्लभ हैं।
गृहस्य श्रियः, गृहदीप्तयः पुण्याः महाभागाश्च स्त्रियः पूजनीयाः उक्ताः (सन्ति)। तस्मात्
(एताः) विशेषतः रक्ष्याः (भवन्ति ॥९॥
अर्थ- घर की लक्ष्मी, घर को प्रकाशित करनेवाली, पुण्या महाभागिनी, स्त्री, पूजनीय हैं। वह विशेष रूप से रक्षा करने योग्य है।
विनयः अकीर्ति हन्ति, पराक्रमः अनर्थं हन्ति, क्षमा नित्यं क्रोधं हन्ति,
आचारः (च) अलक्षणं हन्ति ॥१०॥
अर्थ- विनम्रता अपयश को नाश करता है, पराक्रम अनर्थ को नाश करता है, क्षमा प्रतिदिन क्रोध को नाश करता है, आचरण कुलक्षण को नाश करता है।
शब्दार्थाः
रतिः ↔ आनन्दः ↔ भावुकता
तत्वज्ञः ↔ रहस्यज्ञः ↔ रहस्य को जाननेवाला
योगज्ञः ↔ कौशलं जानाति ↔ कौशल जाननेवाला
उच्यते ↔ कथ्यते ↔ कहा जाता है
उपायज्ञां ↔ उपायं जानाति ↔ उपाय को जाननेवाला
अनाहूत: ↔ न आहूतः ↔ बिना बुलाये हुए
अपृष्टः ↔ न पृष्टः ↔ बिना पूछे हुए
अविश्वस्तं ↔ अविश्वासयोग्ये जने ↔ अविश्वसनीय व्यक्ति पर
मृदचंता ↔ मूर्खः ↔ मूर्ख हृदय वाला
नराधमः ↔ निकृष्टः जनः ↔ मनुष्यों में नीच
सुखावहा ↔ सुखदा ↔ सुख देनेवाली
भूतिम् ↔ ऐश्वर्यम् ↔ ऐश्वर्य को
इच्छता ↔ वाच्छता ↔ चाहते हुए
मुजया ↔ शुद्ध्या (शृङ्गारोपचारेण) ↔ स्वच्छता या उबटन आदि के द्वारा
प्रियवादिनः ↔ मधुरभाषिणः ↔ प्रिय बोलने वाले
अकोर्तिम् ↔ अपयशः ↔ अपयश
हन्ति ↔ नाशयति ↔ नाश करता है।
अलक्षणम् ↔ कुलक्षणम् ↔ कुलक्षण, कुरूपता
अभ्यासः (मौखिकः)
1. एकपदेन उत्तरं वदतः-
(क) विदुरः कः आसीत् ?
उत्तर-मन्त्रिप्रवरं
(ख) मूढचेता नराधमः कस्मिन् विश्वसिति ?
उत्तर-अविश्वस्तं
(ग) उत्तमा शान्तिः का ?
उत्तर-क्षमैका
(घ) का परमा तृप्तिः ?
उत्तर-विद्यका
(ङ) नरकस्य किंयद् द्वारं परिगणितम् ?
उत्तर-त्रिविधं
(च) विद्या केन रक्ष्यते ?
उत्तर-योगेन
(छ) विनयः कं हन्ति ?
उत्तर- अकीर्ति
प्रश्न 2. श्लोकांशं योजयित्वा वदत-
(क) त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः
कामक्रोधस्तया लोभस्तस्मादेतत् त्रयं त्यजेत्।
(ख) सत्येन रक्ष्यते धर्मों विद्या योगेन रक्ष्यते।
उत्तर-मुजया रक्ष्यते रूपं कुलं वृत्तेन रक्ष्यते।।
अभ्यासः (लिखितः)
1. एकपदेन उत्तरं वदत
(क) केषां तत्वज्ञः पण्डितः उच्यते ?
उत्तर- सर्वभूतानां
(ख) अनाहूतः कः प्रविशति ?
उत्तर-मूर्खः
(ग) धर्मः केन रक्ष्यते ?
उत्तर-सत्येन
(घ) क्षमा कं हन्ति ?
उत्तर-क्रोधम्
(ङ) सुखावहा का ?
उत्तर-अहिंसैका
(च) नरकस्य त्रिविधं द्वारं कस्य नाशनम् ?
उत्तर-आत्मनस्य
(छ) केन षड् दोषाः हातव्याः ?
उत्तर-पुरूपेण
2. उदाहरणमनुसृत्य क्तिन् प्रत्यय-योगेन शब्द निर्माणं करणीयम्-
उदाहरणरम् – भू + क्तिन् = भूतिः
प्रश्ना : (क) गम् + क्तिन् = गतिः
शम् + क्तिन् = शान्तिः
तृप् + क्तिन् = तृप्तिः
रम् + क्तिन् = रतिः
श्रम् + क्तिन् = श्रान्तिः
सम् + ऋध् + क्तिन् = समृद्धिः
वृध् + क्तिन् = वृद्धिः
नी + क्तिन् = नीतिः
हन् + क्तिन् = हन्तिः
कृ + क्तिन् = कृतिः
3. उदाहरणानुसारं वाच्य-परिवर्तनं कुरूत-
उदाहरणम् (क) कर्तृवाच्ये – विनयः अकीर्ति हन्ति ।
विनयेन अकीर्तिः हन्यते।
(ख) कर्मवाच्ये धर्मः सत्येन रक्ष्यते।
कर्तृवाच्ये सत्यं धर्म रक्षति।
प्रश्नाः (क) पराक्रमः अनर्थ हन्सि।
उत्तर-कर्मवाच्यः पराक्रमेण अनर्थः हन्यते।
(ख) क्षमया क्रोधः हन्यते।
उत्तर-कर्तृवाच्य – क्षमा क्रोधम् हन्ति ।
(ग) योगः विद्यां रक्षति।
उत्तर-कर्मवाच्य- योगेण विद्या रक्ष्यते।
(घ) मृजया रूपं रश्यते।
उत्तर-कर्तृवाच्य- मृजा रूपम् रक्षति।
(ङ) आचारेण अलक्षणः हन्यते ।
उत्तर-कर्तृवाच्य – आचारः अलक्षणम् हन्ति।
(च) मया ग्रन्थः पठ्यते।
उत्तर-कर्तृवाच्य- अहम् ग्रन्थम् पठति।
(छ) वयं वेदं पठामः।
उत्तर-कर्मवाच्य-अस्मभिः वेदः पठयामहे।
4. पूर्णवाक्येन उतरं लिखत-
(क) पुरूषेण के पड् दोषाः हातव्याः ?
उत्तर-पुरूषेण निद्रा, तन्द्रा, भयं, क्रोध, आलस्यं दीर्घसूत्रता षड् दोषाः हातव्याः।
(ख) पण्डितः कः उच्यते ?
उत्तर-यस्य कृत्यं न विघ्नन्ति शीतमुष्णं भयंरतिः। समृद्धिरसमृद्धिर्वा पण्डित सः उच्यते।
(ग) एक एव धर्मः किं कथ्यते ?
उत्तर-एको धर्मः परं श्रेयः।
(घ) नरकस्य कानि प्रीणि द्वाराणि सन्ति ?
उत्तर-नरकस्य कामः कोधस्तथा लोभः एतानि त्रीणि द्वाराणि सन्ति।
(ङ) कस्य कस्य च वक्ता श्रोता च दुर्लभः ?
उत्तर-अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः।
(च) स्त्रियः गृहस्थ काः उकताः सन्ति ?
उत्तर-गृहस्य श्रियः, गृहदीप्तयः पुण्याः महाभागश्य स्त्रियः पूजनीयाः उक्ताः सन्ति।
(छ) कुलं केन रक्ष्यते ?
उत्तर-कुलं वृत्तेन रक्ष्यते।
5. निम्नांकितपदैः एकैकं वाक्यं रचयत-
(क) उच्यते – सः पण्डितः उच्यते।
(ख) त्यजेत् – रामेण लोभ:त्यजेत्।
(ग) बहुभापते – मूढः अपृष्टो बहुभाषते।
(घ) विश्वसिति – मोहनः विश्वसिति अस्ति।
(ङ) वर्तते – भवान् कुशलम् वर्तते।
(च) विघ्नन्ति-सत्याः कार्यं अनेकानि विध्नन्ति।
(छ) रक्ष्या – पूजनीयाः विशेषतः रक्ष्याः भवन्ति ।
नीतिश्लोकाः पाठ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में हिन्दी में पुछे जाते हैं
1. ‘नीतिश्लोकाः’ पाठ में मूढ़चेता नराधम किसे कहा गया है?
उत्तर : ‘नीतिश्लोकाः’ पाठ में महात्मा विदुर ने मूढ़चेतनराधम के तीन लक्षण बतलाए हैं। ऐसा व्यक्ति जो बिना बुलाए आता है। बिना पूछे ही अधिक बोलता है। वह अविश्वासी पर भी विश्वास करता है।
2. नीतिश्लोकाः पाठ के अनुसार कौन-सा तीन वस्तु त्याज्य है?
उत्तर : नरक के तीन द्वार हैं- काम, क्रोध और लोभ। ये तीनों द्वार अपने-आप को नष्ट कर देता है। इसलिए इन तीनों को त्याग ही देना चाहिए।
3. नीतिश्लोकाः पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है?
उत्तर : नीतिश्लोकाः पाठ महात्मा विदुररचित ‘विदुरनीति’ ग्रंथ से उद्धृत है। इस ग्रंथ में महाभारत तथा भागवतगीता में चित्त को शांत करनेवाले आध्यात्मिक श्लोक हैं। इन श्लोकों में जीवन के यथार्थ पक्ष का वर्णन किया गया है। इससे संदेश. मिलता है कि सत्य ही सर्वश्रेष्ठ है। सत्य के मार्ग से कदापि विचलित नहीं होना चाहिए।
4. ‘नीतिश्लोकाः’ पाठ के आधार पर मनुष्य के छह दोषों का हिन्दी में वर्णन करें।
उत्तर : महात्मा विदुर द्वारा रचित ‘विदुरनीति’ ग्रंथ से संकलित ‘नीतिश्लोकाः’ पाठ में मनुष्य के छह दोषों का वर्णन किया गया है। ये छह दोष -नींद, ऊँघना, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घसूत्रता (किसी काम को विलंब से करने की प्रवृत्ति) हैं। नीतिकार का कहना है कि प्रगति की इच्छा रखनेवाले मनुष्यों को इन छह दोषों को त्याग देना चाहिए, क्योंकि अधिक निद्रा के कारण वह कोई काम, समय पर नहीं कर पाता। वह तंद्रावश प्रत्येक काम में पीछे रह जाता है। भय के कारण काम आरंभ ही नहीं करता तथा क्रोध के कारण बना काम भी बिगड़ जाता है। आलस्य के कारण समय का सदुपयोग नहीं हो पाता, तो दीर्घसूत्रता अथवा काम को कल (आनेवाले समय) पर छोड़ने के कारण काम का बोझ बढ़ जाता है।
5. वैदिक साहित्य किसे कहते हैं?
उत्तर: वेद भारतीय धर्म, दर्शन और संस्कृति के मूल आधार हैं। वेद के अंतर्गत अनेकों ग्रंथ आते हैं जिनको ही वैदिक साहित्य कहा जाता है।
6. ‘नीतिश्लोकाः’ पाठ के आधार पर सुलभ और दुर्लभ कौन हैं?
उत्तर: सदा प्रिय बोलनेवाले, अर्थात् जो अच्छा लगे यही बोलनेवाले मनुष्य सुलभ है। अप्रिय और जीवन की सही मार्ग पर ले जानेवाले वचन बोलने वाले तथा सुनने वाले मनुष्य दोनों ही प्रायः दुर्लभ हैं।
7. ‘नीतिश्लोकाः’ के आधार पर कैसा वोलनेवाले व्यक्ति कठिनाई से मिलते हैं?
उत्तर : ‘नीतिश्लोकाः’ पाठ में विदुर स्पष्ट कहते हैं कि उचित बोलनेवाले व्यक्ति कठिनाई से मिलते हैं और उचित सुननेवाले व्यक्ति भी कठिनाई से मिलते हैं। इसको स्पष्ट करते हुए विदुर कहते हैं कि उचित बोलना प्रिय नहीं होता है तथा अप्रिय बोलकर कोई भी व्यक्ति किसी का शत्रु नहीं बनना चाहता है। दोनों अतएव विदुर के अनुसार दुर्लभ हैं।
8. नीच मनुष्य कौन है? पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें।
उत्तर: नीच मनुष्य का अभिप्राय निम्न जाति में जन्म लेने वाले से नहीं है। सत् और असत् कर्मों में संलग्न रहने वाला मनुष्य भी नीच की श्रेणी में नहीं आता है। जो बिना बुलाये हुए किसी सभा में प्रवेश करता है, बिना पूछे हुए बहुत बोलता है, नहीं विश्वास करने पर भी बहुत विश्वास करता है। ऐसा पुरुष ही नीच की श्रेणी में आता है।
9. ‘नीतिश्लोकाः’ पाठ के आधार पर पण्डित के लक्षण क्या हैं?
उत्तर : जिसके कर्म को सर्दी-गर्मी, भय-आनंद, उन्नति अवनति बाधा नहीं डालते हैं, उसे ही पंडित कहते हैं। इतना ही नहीं, सभी जीवों के रहस्य को जाननेवाला तथा सभी कर्मों के कौशल को जाननेवाला पंडित कहलाता है। मनुष्यों में उपाय जाननेवाला भी पंडित कहलाता है।
10. नीतिश्लोकाः पाठ के आधार पर स्त्रियों की क्या विशेषताएँ हैं?
उत्तर : स्त्रियाँ घर की लक्ष्मी हैं। ये पूजनीया तथा महाभाग्यशाली है। ये पुण्यमयी और घर को प्रकाशित करनेवाली कही गई हैं। अतएव, स्त्रियाँ विशेषरूप से रक्षा करने योग्य होती हैं।
11. उन्नति की इच्छा रखनेवाले मनुष्यों को क्या करना चाहिए?
उत्तर : उन्नति की इच्छा रखनेवाले मनुष्यों को निद्रा (अधिक सोना) तथा तंद्रा (ऊँधना) को त्याग देना चाहिए। इतना ही नहीं भय, क्रोध, आलस्य और काम (वासना) को टालने की प्रवृत्ति भी रखना चाहिए। इस पाठ में महात्मा विदुर का कथन है कि ये छह दोष मनुष्य को आगे बढ़ने में बाधक हैं।
12. नरक के तीन द्वार कौन-कौन से हैं?
उत्तर: नरक के तीन द्वार हैं- काम, क्रोध और लोभ। ये तीनों द्वार अपने-आप को नष्ट कर देता है। इसलिए इन तीनों को त्याग ही देना चाहिए।
13. ‘नीतिश्लोकाः’ पाठ के आधार पर ‘मूढ़चेता नराधम्’ के लक्षणों को लिखें।
उत्तर : ‘नीतिश्लोकाः’ पाठ में महात्मा विदुर ने मूढ़चेतनराधम के तीन लक्षण बतलाए हैं। ऐसा व्यक्ति जो बिना बुलाए आता है। बिना पूछे ही अधिक बोलता है। वह अविश्वासी पर भी विश्वास करता है।
14. ‘नीतिश्लोकाः’ पाठ से किसी एक श्लोक को साफ-साफ शब्दों में लिखें।
उत्तर : सत्येन रक्ष्यते धर्मों विद्या योगेन रक्ष्यते। मृजया रक्ष्यते रूपं कुलं वृत्तेन रक्ष्यते ।।