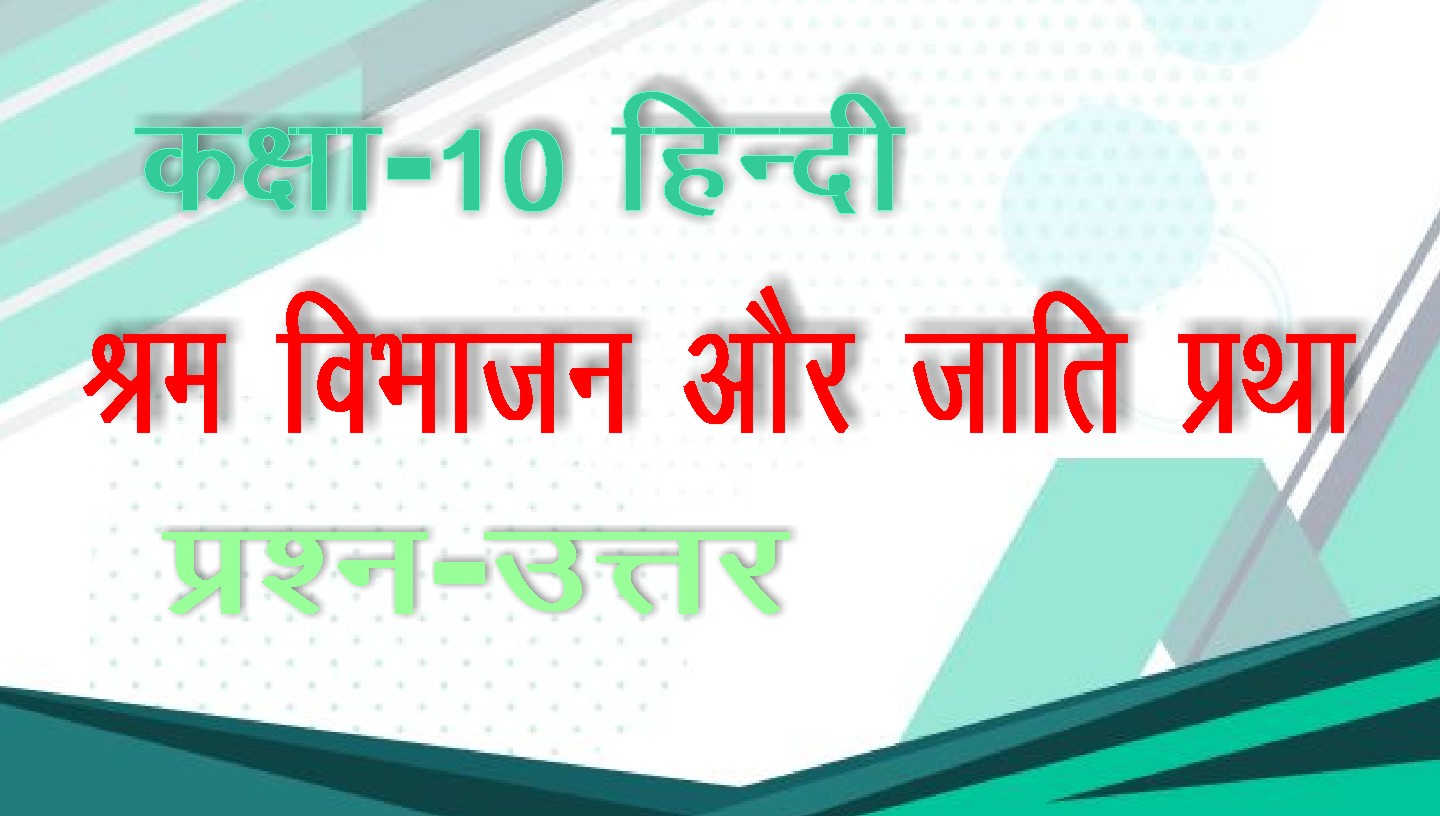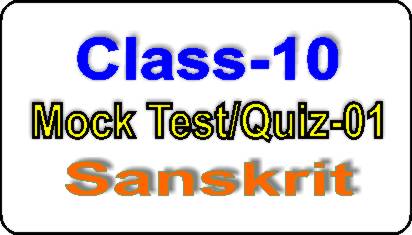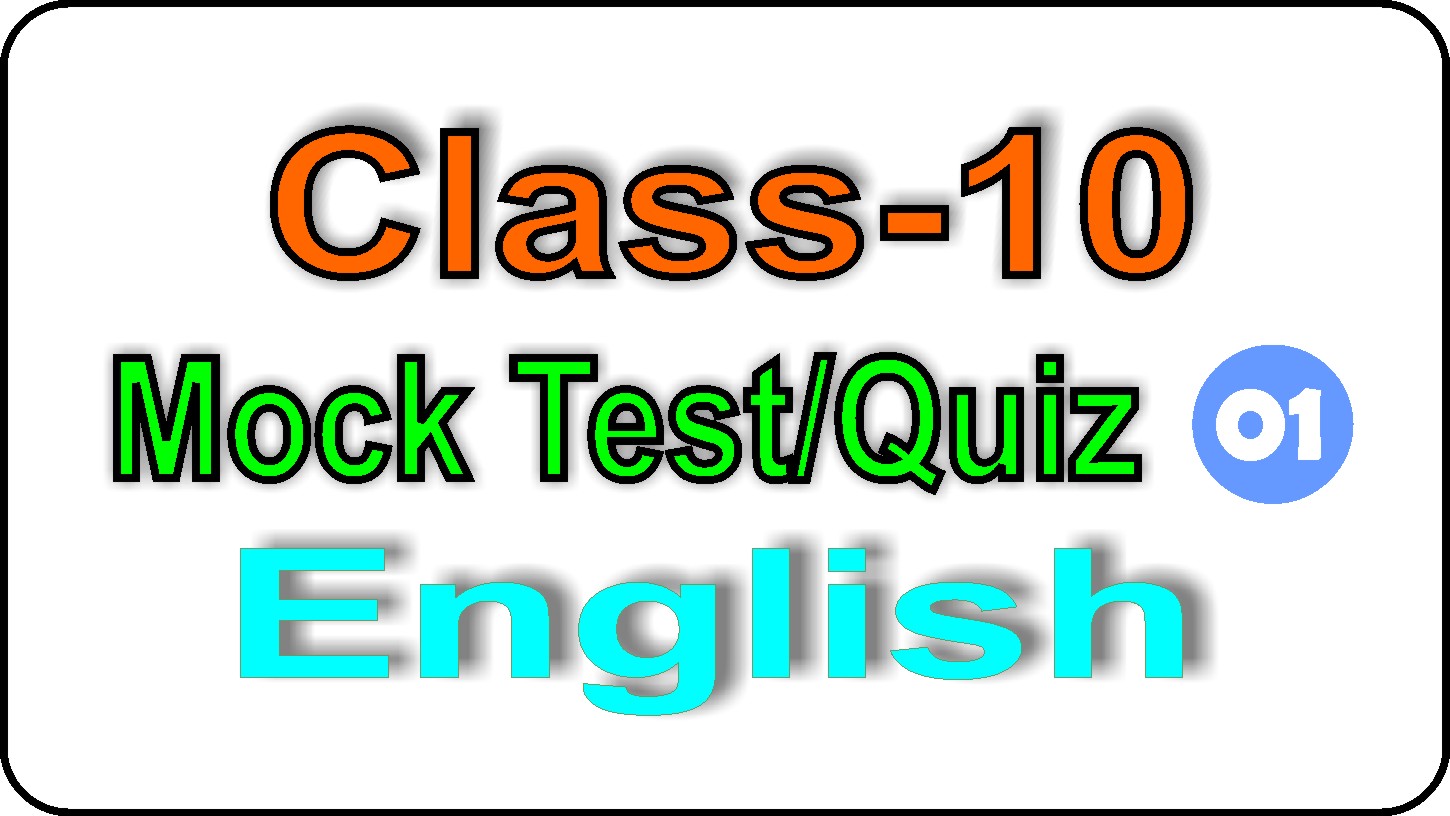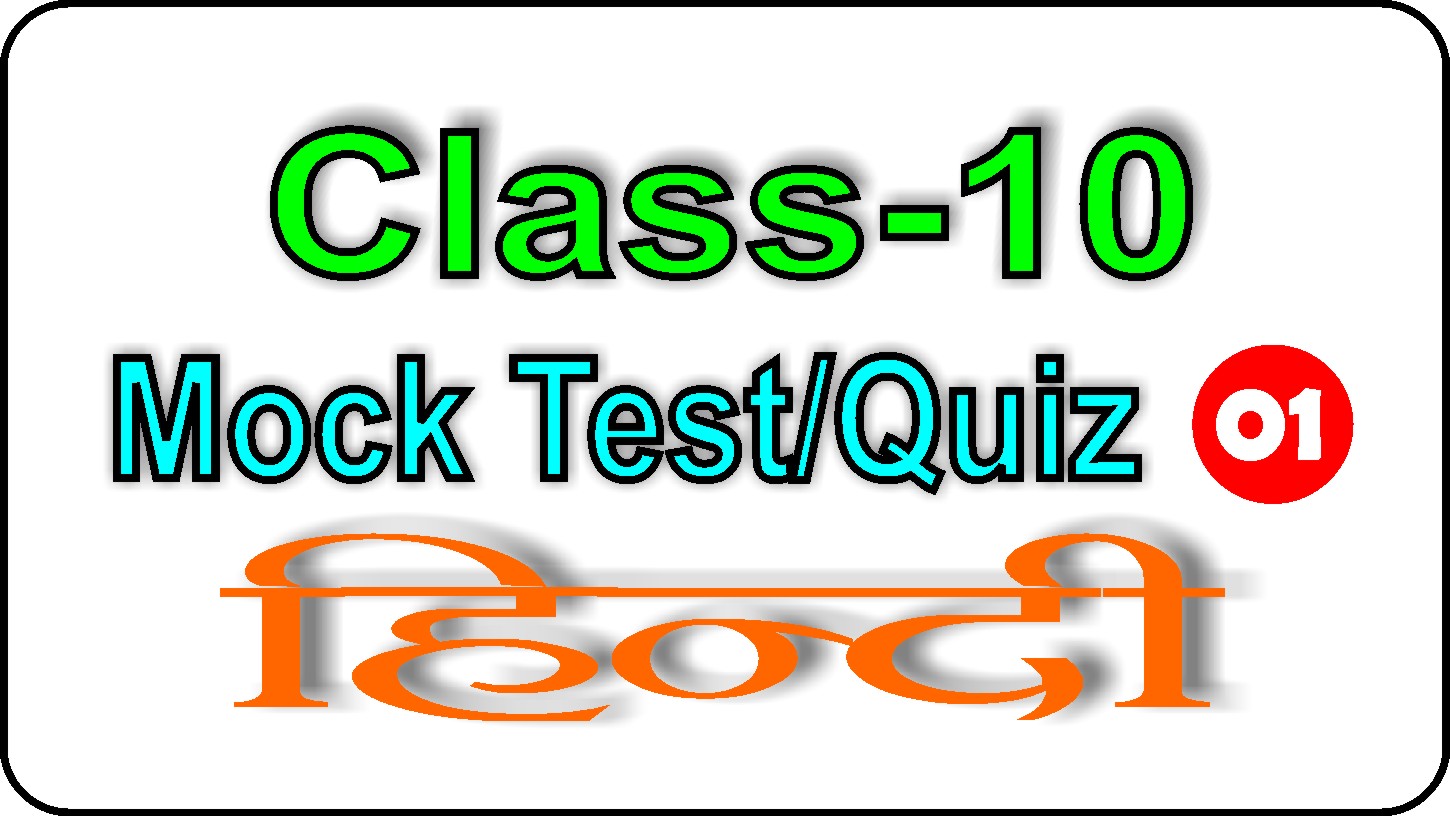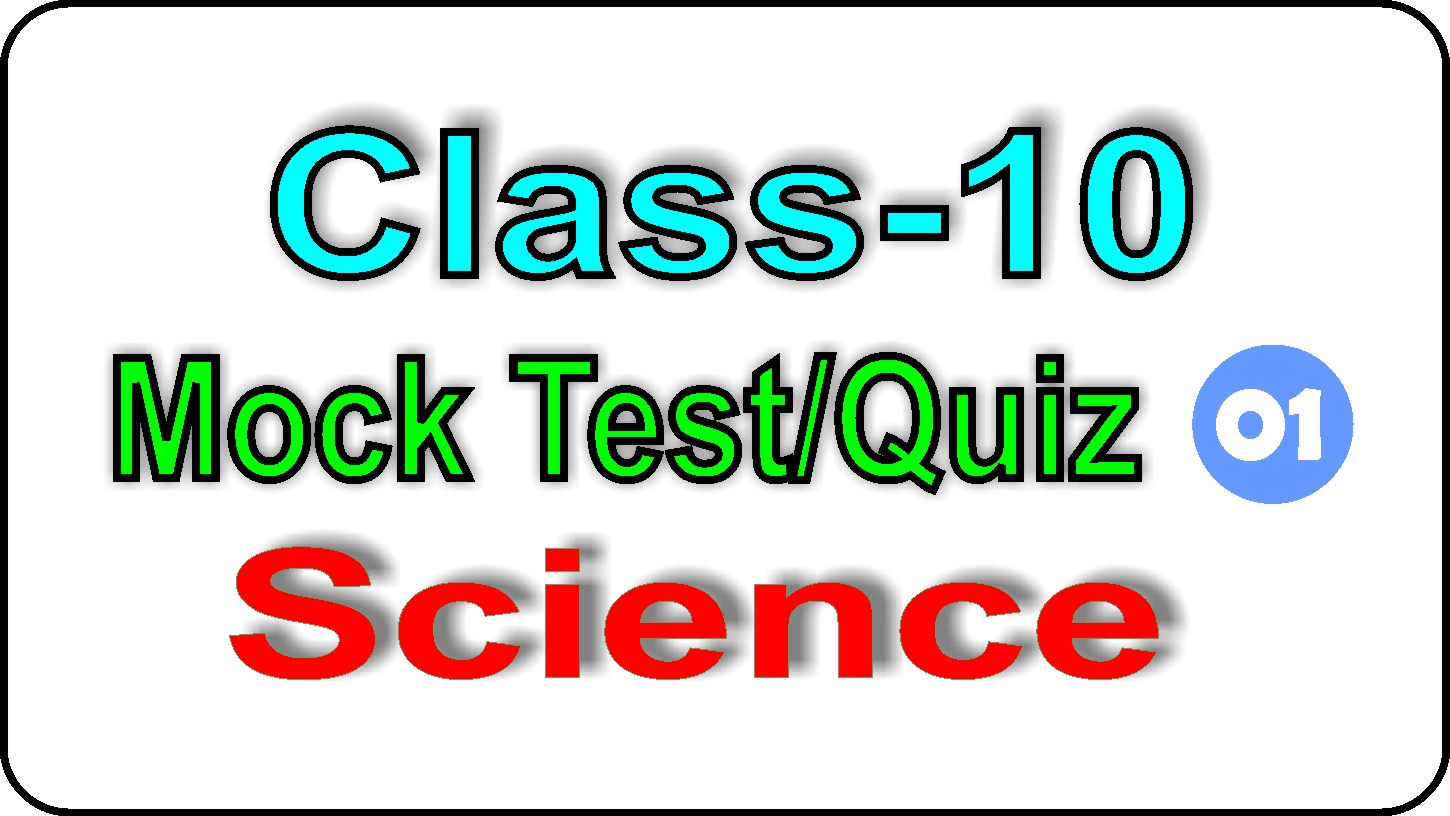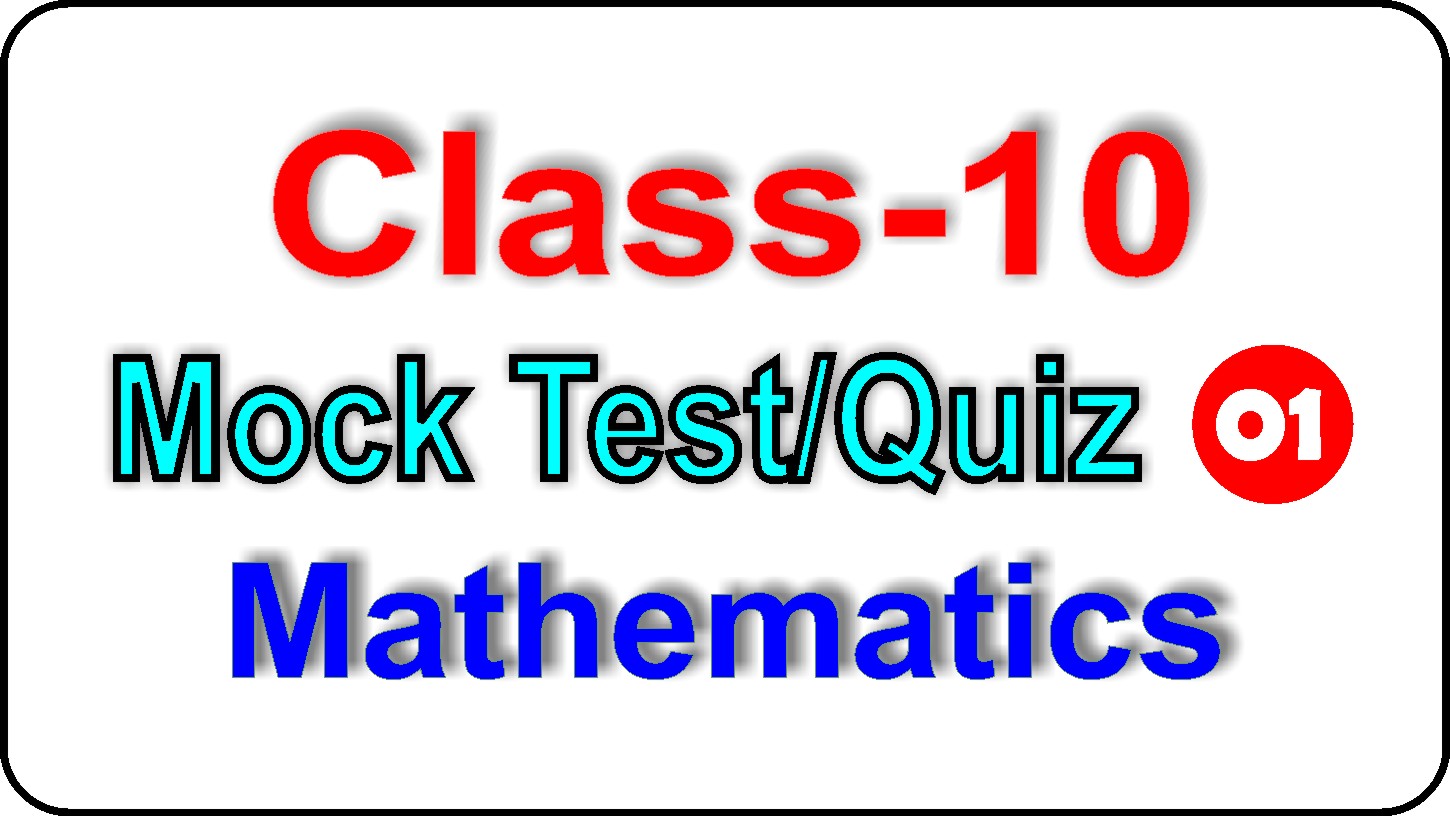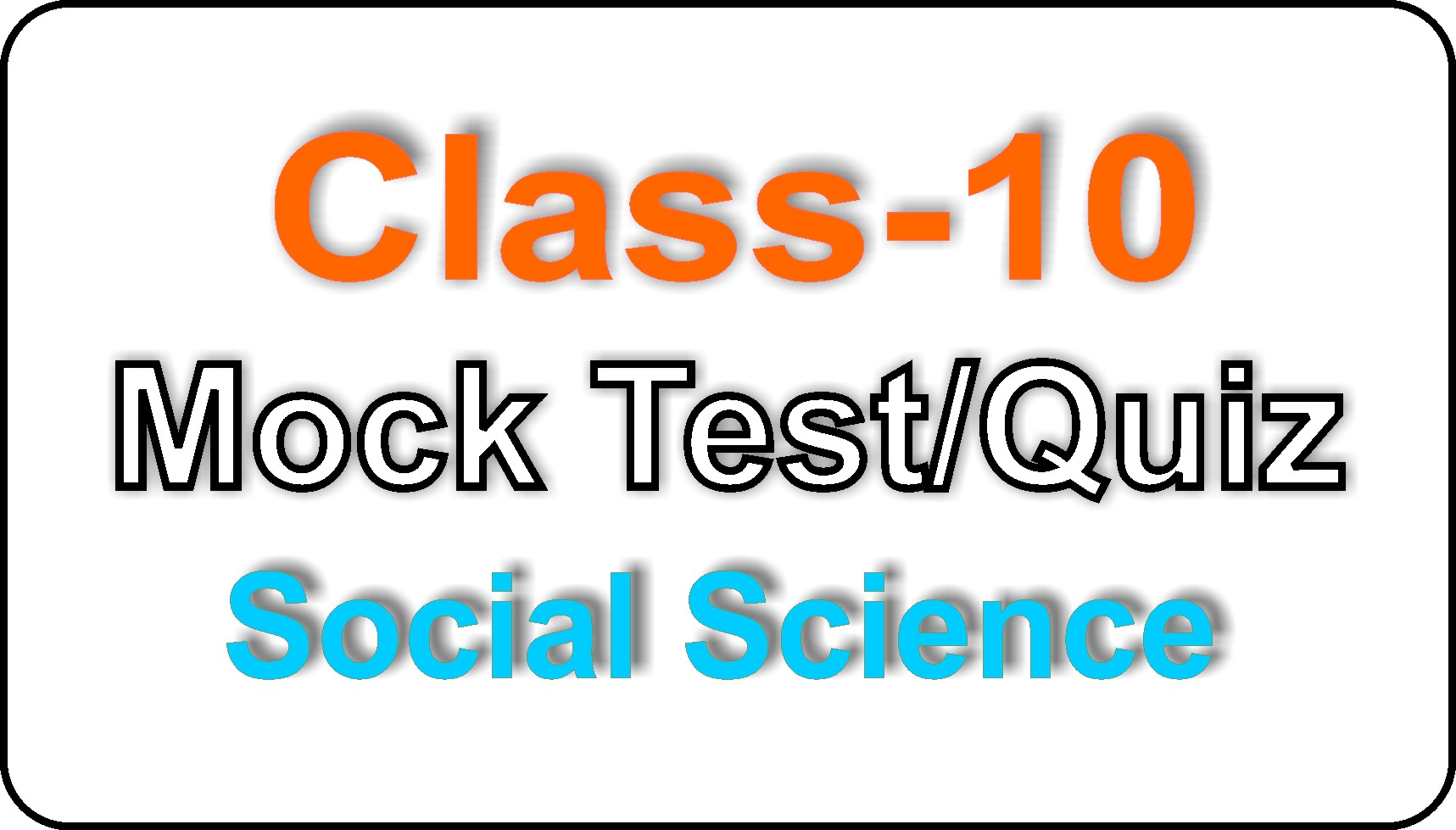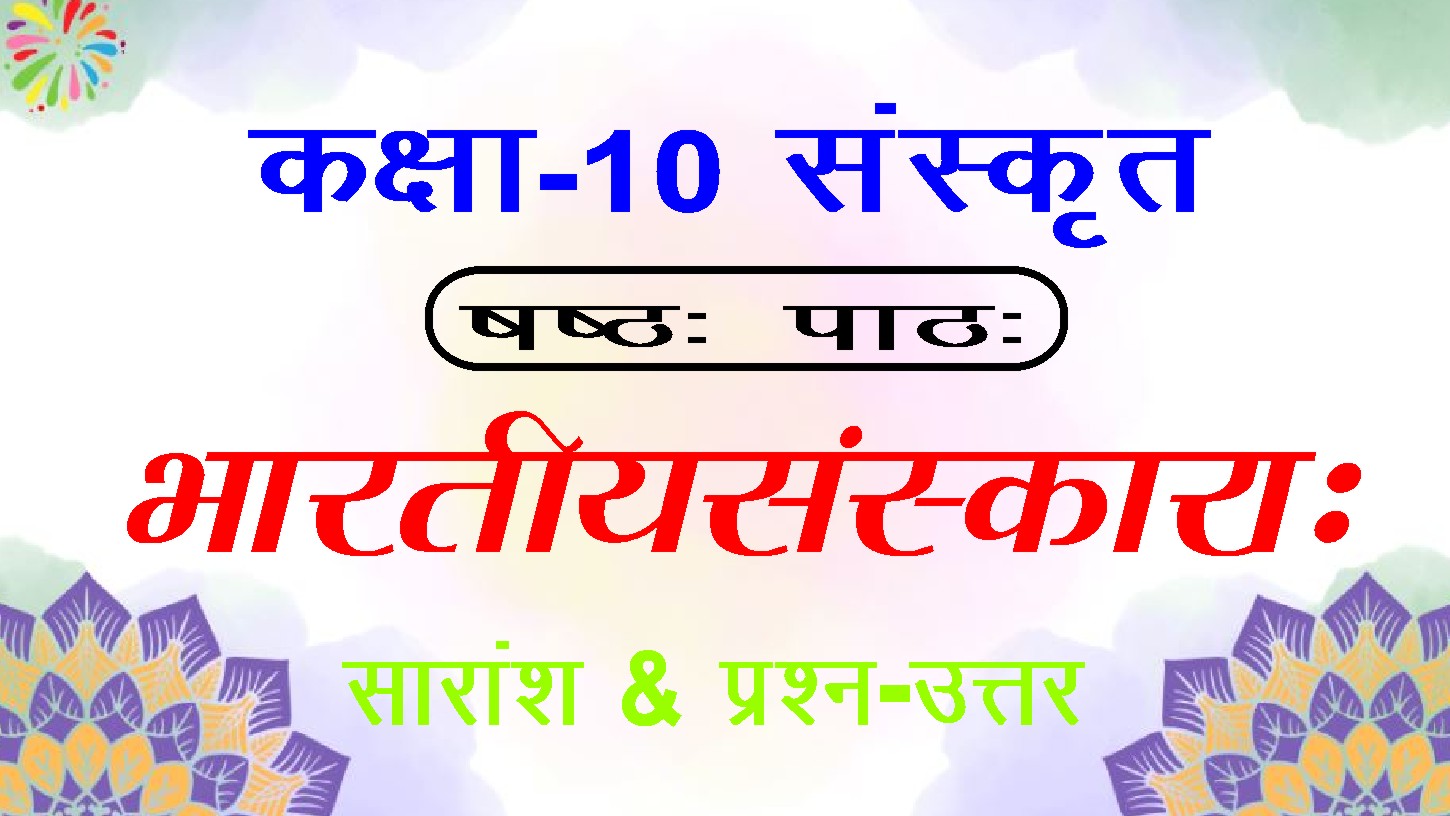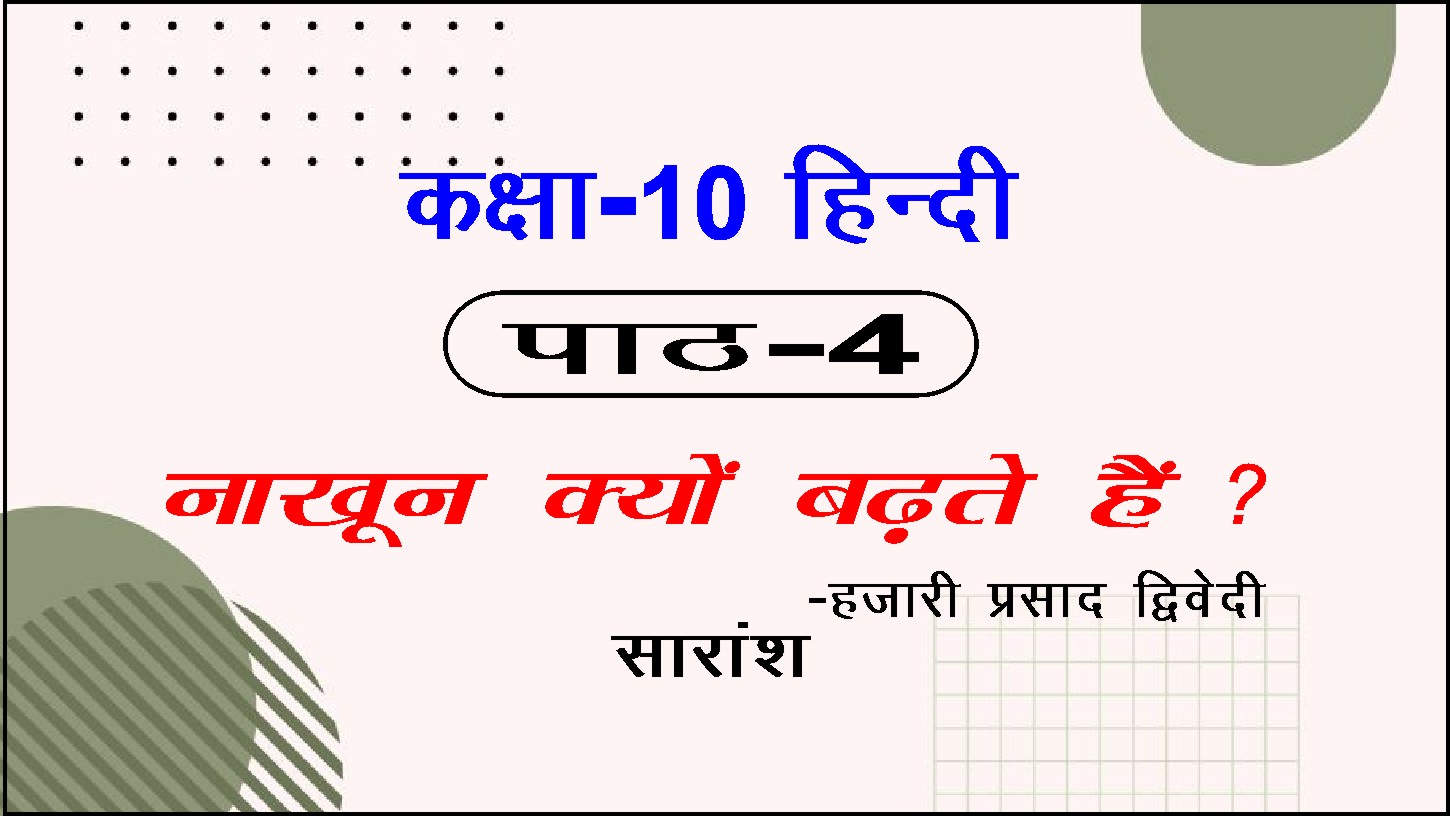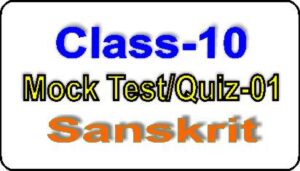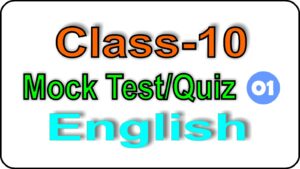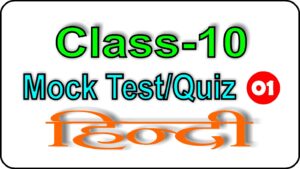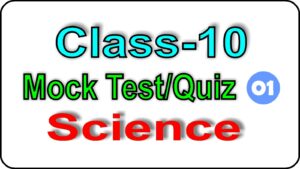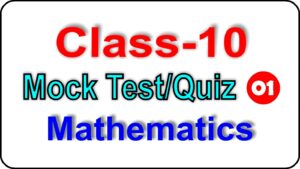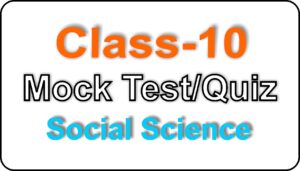दोस्तों इस पोस्ट में आपको बिहार बोर्ड Class 10 Hindi Chapter 1 श्रम-विभाजन और जाति-प्रथा से जीतने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन सकता है जिसे आने वाले बोर्ड परीक्षा मे पुछे जाने की संभावना है सभी को यहाँ शामिल करने की कोशिश किया गया है जिसे याद करके आप करके अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हो और परीक्षा में अच्छे अंक ला सकते हो| अगर आपलोग गणित की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल Unlock Study पर जा कर देख सकते हैं वहाँ पूरे गणित का प्रश्नावली का playlists बना हुआ हैं|
श्रम-विभाजन और जाति-प्रथा
◊भीमराव अंबेदकर
लेखक परिचय:- बाबा साहेब भीमराव अंबेदकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ई० में महू, मध्यप्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उत्त्वतर शिक्षा के लिए न्यूयार्क (अमेरिका), फिर वहाँ से लंदन (इंग्लैंड) गए। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वाङ्मय अनुवाद के जरिये पढ़ा और ऐतिहासिक-सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएँ प्रस्तुत कीं। सब मिलाकर वे इतिहास मीमांसक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद् तथा धर्म-दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे । स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की। समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। उनके चिंतन व रचनात्मकता के मुख्यतः तीन प्रेरक व्यक्ति रहे बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले । भारत के संविधान निर्माण में उनकी महती भूमिका और एकनिष्ठ समर्पण के कारण ही हम आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कह कर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दिसंबर, 1956 ई० में दिल्ली में बाबा साहेब का निधन हो गया।
रचनाएँ:- ‘द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म’, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट’, ‘द अनटचेबल्स, हू आर दे’, ‘हू आर शूद्राज’, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म’, बुद्धा एण्ड हिज धम्मा’, ‘थाट्स ऑन लिंग्युस्टिक स्टेट्स’, ‘द राइज एंड फॉल ऑफ द हिन्दू वीमेन’, ‘एनीहिलेशन ऑफ कास्ट’ आदि ।
पाठ का सारांस:- प्रस्तुत पाठ बाबा साहेब का प्रसिद्ध भाषण “एनीहिलेशन ऑफ कास्ट” से लिया गया। जिसको जाति-पाँति तोड़क मंडल” (लाहौर) के वार्षिक सम्मेलन में पढ़ने के लिए बाबा साहेव ने लिखा था । भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए यह आलेख अत्यन्त शिक्षाप्रद है ।
यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी “जातिवाद” के पोषकों की कमी नहीं है। उनके समर्थन के अनेक आधार हैं-
पहला आधार “आधुनिक सभ्य समाज” “कार्य-कुशलता” के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है और जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं ।” जातिवाद के समर्थकों के इस तर्क के खण्ड़न में बाबा साहेब ने आपत्ति दर्शाई है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ-साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए हैं।
सभ्य समाज में श्रम विभाजन व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता। भारत की जाति प्रथा श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं बल्कि विभाजित ‘वर्गों का एक-दूसरे की अपेक्षा ऊँचा नीचा भी करा देती है जो विश्व के किसी समाज में नहीं मिलता है।
भारतीय श्रम विभाजन मनुष्य की रुचि के आधार पर श्रम विभाजन नहीं उसके कार्य-कुशलता या सक्षमता के आधार पर नहीं बल्कि आज का भारतीय श्रम विभाजन जातिगत के आधार पर है। बच्चा गर्भ में रहता है उसी समय उसके लिए श्रम विभाजन कर दिया जाता है जो जीवन भर माता-पिता के आधार लेकर पेशा का निर्धारण कर लेता है। चाहे वह उस पेशा में कुशल हो या न हो। उसकी रुचि उस पेशा में हो या नहीं हो। वह भले ही अकुशलता के कारण भूखे मर जाय ।
भारतीय जाति प्रथा प्रतिकूल परिस्थितियों में भी किसी व्यक्ति को पेशा चुनने का अधिकार नहीं देती जो भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण बना हुआ है।
श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा द्वारा किया गया श्रम विभाजन मनुष्य के स्वेच्छा पर निर्भर नहीं है। जो लोग अपना कार्य ‘अरुचि’ या विवशता से करते हैं उनका दिल-दिमाग काम में नहीं लगता है, फिर उन्हें कुशलता कैसे प्राप्त होगी । इस प्रकार हो सकता है कि जातिवाद द्वारा किया गया श्रम विभाजन स्वभाविक नहीं बल्कि अस्वाभाविक हैं जो मनुष्य को निष्क्रिय बना देती है।
बाबा साहेब के अनुकूल आदर्श समाज के लिए स्वतंत्रता, समता और भाईचारे का होना आवश्यक है। क्योंकि आदर्श समाज में गतिशीलता होनी चाहिए जो समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचालित रहे। आदर्श समाज में बहुविध हितों में सबको समान भागीदारी होना चाहिए । इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति नहीं है, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान-प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो ।
1. बाबा साहेव भीमराव अंबेदकर का जन्म कब हुआ था ?
(A) 14 अप्रैल, 1891 ई० में
( B) 20 अप्रैल, 1892 ई में
(C) 24 अप्रैल, 1893 ई० में
(D) 28 अप्रैल, 1894 ई० में
(A) 14 अप्रैल, 1891 ई० में
2. “श्रम-विभाजन और जाति प्रथा’ के लेखक कौन हैं?
(A) भीमराव अंबेदकर
(B) रामविलास शर्मा
(C) गुणाकर मुले
(D) हजारी प्रसाद द्विवेदी
उत्तर :(A) भीमराव अंबेदकर
3. बाबा साहेव भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ?
(A) बिहार
(B) मध्यप्रदेश
(C) गुजरात
(D) महाराष्ट्र
उत्तर : (B) मध्यप्रदेश
4. ‘श्रम विभाजन और जाति प्रथा’ पाठ वावा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है?
(A) द कास्ट्स इन इंडिया: देयर मैकेनिज्म
(B) जेनेसिस एंड डेवलपमेंट
(C) एनीहिलेशन ऑफ कास्ट
(D) हू आर शूद्राज
उत्तर : (C) एनीहिलेशन ऑफ कास्ट
5. जाति प्रथा और श्रम विभाजन क्या है?
(A) कहानी
(B) शिक्षा शास्त्र
(C) रिपोतार्ज
(D) निबंध
उत्तर : (D) निबंध
6. डॉ० भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है?
(A) सती-प्रथा
(B) दहेज-प्रथा
(C) बाल विवाह-प्रथा
(D) जाति-प्रथा
उत्तर : (C) बाल विवाह-प्रथा
7. भारत में वेरोजगारी का मुख्य कारण है?
(A) जाति प्रथा
(B) दहेज प्रथा
(C) अशिक्षा
(D) भ्रष्टाचार
उत्तर : (A) जाति प्रथा
8. बावा साहव भीमराव अंबेडकर एक भी थे?
(A) गायक
(C) संगीतकार
(B) अभिनेता
(D) वकील
उत्तर : (D) वकील
9. लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था ?
(A) 1935
(B) 1936
(C) 1835
(D) 1836
उत्तर : (C) 1835
10. “बाबा साहेव अम्बेडकर संपूर्ण वाड्मय” नाम की पुस्तक कितने खण्डों में प्रकाशित हो गई है?
(A) 22
(B) 48
(C) 21
(D) 20
उत्तर : (C) 21
11. जाति प्रथा भारत में क्यों एक प्रमुख कारण बनी है?
(A) उत्पीड़न
(B) बेरोजगारी
(C) अमीरी
(D) गरीबी
उत्तर : (B) बेरोजगारी
12. भीमराव अम्बेडकर के चिंतन और रचनात्मकता के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति रहे ?
(A) 5
(B) 8
(C) 10
(D) 3
उत्तर : (D) 3
13. सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है?
(A) जाति-प्रथा
(B) श्रम-विभाजन
(C) अणु-बम
(D) दूध-पानी
उत्तर : (B) श्रम-विभाजन
14. जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ-साथ किसका रूप लिए हुए है?
(A) स्वतंत्रता का
(B) भ्रातृत्व का
(C) श्रमिक विभाजन का
(D) इनमें से कोई नहीं
उत्तर : (C) श्रमिक विभाजन का
15. आधुनिक सभ्य समाज में कार्य-कुशलता के लिए किसको आवश्यक माना गया है?
(A) जाति-प्रथा
(B) कार्य-कुशलता
(C) वर्ण-विभाजन
(D) श्रम-विभाजन
उत्तर : (D) श्रम-विभाजन
16. भीमराव अम्बेडकर के प्रेरकों के क्या-क्या नाम थे ?
(A) राम, कबीर, सहात्मा गाँधी
(B) बुद्ध, रहीम, कबीर
(C) बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले
(D) कबीर, बुद्ध, महादेवी वर्मा
उत्तर : (C) बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले
17. ‘पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो इसके लिए भूखों मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है?’ उक्त पंक्ति किस पाठ से ली गई है?
(A) श्रम विभाजन और जाति-प्रथा
(B) बहादुर
(C) शिक्षा और संस्कृति
(D) आविन्यों
उत्तर : (A) श्रम विभाजन और जाति-प्रथा
18. सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानता है?
(A) कार्य-कुशलता
(B) जाति प्रथा
(C) वर्ण-विभाजन
(D) उपरोक्त कोई नहीं
उत्तर : (A) कार्य-कुशलता
19. भारतीय संविधान के निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका किसकी है?
(A) भीमराव अंबेदकर
( B) ज्योतिबा फुले
(C) राजगोपालाचारी
(D) महात्मा गाँधी
उत्तर : (A) भीमराव अंबेदकर
20. भीमराव अम्बेदकर की निधन कब और कहाँ हुआ था ?
(A) जनवरी 1965, मध्य प्रदेश
(B) दिसम्बर 1956, दिल्ली
(C) फरवरी 1914, गोवा
(D) मार्च 1865, उड़ीसा
उत्तर : (B) दिसम्बर 1956, दिल्ली
लघु /दीर्घ उत्तरीये प्रश्न
1. लेखक किस विडम्बना की बात करते हैं ? विडम्बना का स्वरूप क्या हैं?
उत्तर : इस पाठ में लेखक भारत में व्यापक रूप से फैले जाती प्रथा की बात करते हैं। विडम्बना का स्वरूप : भारतीय जातिप्रथा पेशे का पूर्वनिर्धारण करती है और मनुष्य को जीवनभर के लिए एक पेशे से बाँध देती है। वह पेशा भले ही उस मनुष्य के जीवनयापन के लिए अपर्याप्त और अनुपयुक्त ही क्यों न हो, उसे उसी में बँधने की विवशता है।
2. जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं?
उत्तर : जातिवाद के पक्ष में इसके पोषकों का तर्क है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य-कुशलता के लिए श्रम-विभाजन को आवश्यक माना जाता है और जाति-प्रथा भी श्रम-विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है।
3. जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियाँ क्या हैं?
उत्तर : लेखक (भीमराव अंबेदकर) ने जातिवादियों (जातिवाद के पोषकों) के तर्क को आपत्तिजनक कहा है। जातिप्रथा में श्रम विभाजन के साथ-साथ श्रमिक विभाजन भी है। लेखक की दृष्टि में यही आपत्तिजनक स्थिति है।
4. जाति भारतीय समाज में श्रम-विभाजन का स्वभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती ?
उत्तर : भारतीय समाज में जाति श्रम-विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। इसमें मनुष्य की निजी क्षमता का विचार किए बिना उसका पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। इस प्रकार की प्रथा प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा की स्वतंत्रता प्रदान नहीं करती है।
5.जातिप्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारणक्यों बनी हुई है ?
उत्तर : भारत में प्रचलित जातिप्रथा किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के अनुकूल पेशा चुनने की स्वतंत्रता नहीं देती। इस प्रथा में प्रत्येक व्यक्ति अपने पैतृक पेशा से बँधने को विवश है। पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर भारतीय जातिप्रथा बेरोजगारी का प्रमुख तथा प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। इच्छानुसार पेशा परिवर्तन की स्वतंत्रता होती तो शायद इतनी बेरोजगारी नहीं होती।
6. लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों ?
उत्तर : आज के उद्योगों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि अधिसंख्य लोग ऐसे कार्यों से जुड़े होते हैं जिनमें उनकी कोई रुचि नहीं होती। वे जीवनयापन के लिए ही वैसे कार्यों से जुड़े होने को विवश हैं।
7. लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति-प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है?
उत्तर : जाति-प्रथा में श्रम-विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। इसमें मानवीय कार्यकुशलता की वृद्धि नहीं हो पाती, इसमें स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर कम और टालू कार्य करने को विवश होना पड़ता है। इस प्रथा में मनुष्य निष्क्रिय हो जाता है। इन बातों के माध्यम से लेखन ने आर्थिक पहलू से भी जाति-प्रथा को हानिकारक सिद्ध किया है। साथ ही ऐसी प्रथा में समता, भ्रातृत्व एवं स्वतंत्रता नहीं होता जिससे समझा जा सकता है कि जाति-प्रथा रचनात्मक पहलू से भी हानिकारक है।
8. सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है?
उत्तर : डॉ० भीमराव अंबेडकर के अनुसार सच्चे लोकतंत्र के लिए जातिविहीन, समतामूलक समाज की स्थापना पर बल देना चाहिए। शिक्षा का प्रसार, सबमें भाईचारा आदि का भावना सच्चे लोकतंत्र के लिए आवश्यक शर्त है क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ शासन पद्धति नहीं है, बल्कि सामूति जीवनचर्या की एक पद्धति है। अतः आवश्यक है कि सबमें एक-दूसरे के प्रति सम्मान हो।
Youtube Channel:- Unlock Study